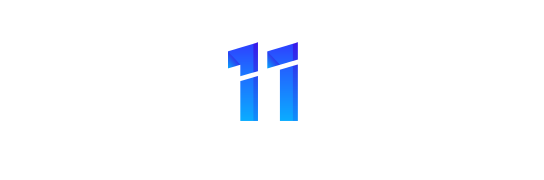फिल्मों का दौर कोई भी रहा हो इंडस्ट्री में ऐसे निर्देशकों की कमी कभी नहीं रही है जिन्होंने अपने दौर में चल रहे फिल्मी फॉर्मूले से अलग हटकर एक नए तरह का सिनेमा रचने का प्रयास न किया हो। यह प्रयास टिकट खिड़की पर प्रदर्शन कैसा करते हैं इसकी परवाह किए बगैर यह फिल्म निर्देशक फिल्मों की चल रही और घिसी-पिटी लय और ताल को बदलने के लिए गंभीर दिखे।
हालांकि इन फिल्मों की आलोचना भी यह कहकर होती रही कि ऐसी फिल्में देखने वाला वर्ग मुट्ठी पर है। पर यह जुमले इन फिल्म निर्देशकों को निराश न करते। ऐसे फिल्मकारों की फिल्में चाहे व्यवसाय भले ही मुख्य धारा की फिल्मों जैसा न कर पायी हों लेकिन भारतीय सिनेमा की पहचान की बात आने पर यह फिल्में हमेशा अगली कतार में हमेशा खड़ी दिखीं।
आइए नजर डालते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दस ऐसे निर्देशकों पर जिन्होंने प्रचलित सिनेमा से अलग हटकर कुछ बनाने का प्रयास किया।
बासु चैटर्जी
बासु चैटर्जी ने 70 और 80 के दशक में फिल्में बनायी हैं। उनकी फिल्मों की खासियत उनका कैनवास है। बासु चैटर्जी की कोई भी फिल्म उठा लीजिए उसके पात्र मध्यमवर्गीय परिवार से होंगे। एक हंसते-खेलते परिवार से बासु कॉमेडी भी उठाते और ड्रामा भी। यह फिल्में दर्शकों को उनकी अपनी फिल्में लगतीं। यह फिल्में तब बनायी गयीं जब पर्दे पर यथार्थ की स्थितियों से बहुत दूर जाकर सिनेमा रचने का लोकप्रिय चलन था। ऑफबीट फिल्मों के बड़े हीरो अमोल पालेकर उनके फेवरेट थे।
बासु चैटर्जी ने कई फिल्में अमोल के साथ कीं। ‘रजनीगंधा’, ‘बातों बातों में’, ‘चितचोर’ और ‘एक छोटी सी बात’ जैसी सफल फिल्मों में हीरो अमोल पालेकर थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर बासु चैटर्जी द्वारा बनायी ‘दिल्लगी’ फिल्म आज भी बेस्ट सिचुवेशल कॉमेडी और ड्रामा के रूप में याद की जाती है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चैटर्जी ने इसी नाम से फिल्म बनायी। ‘खट्टा मीठा’ और ‘शौकीन’ फिल्में भी यह दिखाती रहीं कि कैसे थोड़े से बदलाव के साथ चल रहे सिनेमा को खूबसूरत बनाया जा सकता है।
बासु भट्टाचार्य
बासु भट्टाचार्य एक फिल्म मेकर के साथ एक कुशल समाजशास्त्री भी थे। उनकी फिल्मों में समाज के प्रति उनके निष्कर्श दिख जाया करते हैं। बासु भट्टाचार्य ने ‘अनुभव’, ‘तीसरी कसम’ और ‘आविष्कार’ जैसी फिल्में बनायीं। 1997 में उनके द्वारा बनायी गयी फिल्म ‘आस्था’ इस बात का संकेत थी कि उन्हें अपने समय से आगे का सिनेमा रचना आता है।
दो दशक से अधिक समय तक फिल्मों में सक्रिय रहे बासु भट्टाचार्य ने अपने फिल्म मेकिंग स्टाईल में कई प्रयोग किए। ‘पंचवटी’, ‘मधुमती’ और ‘गृह प्रवेश’ फिल्में बहुत सफल तो नहीं रहीं पर हर फिल्म एक मुद्दे पर विमर्श करती जरूर दिखी। बासु भट्टाचार्य का सिनेमा इस बात की तरफ हमेशा से ही इशारा करता रहा है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए न तो बनायी जानी चाहिए और न ही देखी।
मणि कौल
मणि कौल एक अलग तरह के फिल्मकार थे। पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाना न तो मणि कौल का मकसद था न ही उनका हुनर। उनकी हर फिल्म सिनेमा के दायरे को पुनः परिभाषित करती। हिंदी फिल्मों में ऑफबीट फिल्मों के पुरौधाओं में मणि कौल का नाम सबसे ऊपर पंक्ति में आता है। मणि कौल की शुरुआत उनकी फिल्म ‘उसकी रोटी’ से होती है। इस फिल्म से मणि कौल संकेत दे देते हैं कि वह कैसी फिल्में बनाने के लिए यहां आए हैं।
साहित्य के प्रति मणि कौल का अनुराग जब तब उनकी फिल्मों में दिखता है। ऋतिक घटक के छात्र रहे मणि कौल ने ‘दुविधा’, ‘घासीराम कोतवाल’, ‘सतह से उठता आदमी’, ‘अषाढ़ का एक दिन’ जैसी फिल्में बनायीं। ज्यादातर फिल्में किसी न किसी साहित्य रचना से प्रेरित या उस पर आधारित रही हैं। साहित्य और सिनेमा अद्भुत संगम थीं मणी कौल की फिल्में।
मृणल सेन
सिनेमा रचने के मामले में मृणाल सेन की भी एक लंबी रेंज रही है। उनकी फिल्म बनाने की शैली ने हिन्दी सिनेमा पर भी काफी असर डाला। ‘कलकत्ता 71’, ‘भुवन सोम’, ‘एकदिन प्रतिदिन’ और ‘मृगया’ उनकी चर्चित फिल्में रहीं हैं। मृणाल सेन ने 30 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। उनकी फिल्मों की ख्रासियत उस समय के समाज का अक्स उनकी फिल्मों में दिखना होता था।
यह समाज के प्रति एक फिल्मकार की अघोषित जवाबदेही थी। मृणाल सेन ने ‘एक अधूरी कहानी’, ‘चलचित्र’, ‘एक दिन अचानक’ जैसी अलग किस्म की फिल्में भी रचीं। यह फिल्में उस समय बन रही ज्यातर फिल्मों से विषय के मामले में पूरी तरह से अलग होतीं। मृणाल सेन ने जिन 6 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है वह भी विषय के स्तर पर अलग तरह की फिल्में रहीं हैं।
सई परांजपे
सई परांजपे की फिल्म मेकिंग स्टाईल की विशेषता उसकी बुनावट और शिल्प है। उनकी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक न के बराबर होता है। दर्शक जब सई परांजपे की फिल्में देख रहा होता है तो वह फिल्म के पात्रों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। कॉमेडी फिल्म ‘चश्मेबदूर’ बनाने के साथ सई ने ‘कथा’, ‘स्पर्श’ और ‘दिशा’ जैसी फिल्में बनायीं।
इन सभी फिल्मों की खासियत फिल्म की संवेदनशीलता रही है। उनकी फिल्म का हर पात्र दर्शकों को खुद की जिंदगी का ही एक हिस्सा लगता। बॉक्स ऑफिस पर ‘चश्मेबदूर’ को छोड़कर कोई भी फिल्म बड़ी सफल साबित नहीं हुई लेकिन उनकी सफलता इस बात में थी कि उन्होंने इंडस्ट्री को बताया कि इस तरह की फिल्में भी बनायी जा सकती हैं।
श्याम बेनेगल
श्याम बेनेगल का सिनेमा चिंता और सरोकारों का सिनेमा है। उनकी हर फिल्म किसी चिंता के प्रति दर्शकों को जागरुक करने की कोशिश करती है। फिर वह चाहे ‘अंकुर’ हो या फिर ‘वेलडन अब्बा’। श्याम बेनेगल की खासियत रही है कि उनके सामाजिक सरोकारों वाला सिनेमा वक्त के साथ अपने विषय बदलता रहा है, ताकि वह रिलीवेंट बने रहे।
‘निशांत’, ‘भूमिका’, ‘आरोह’, ‘मंथन’, ‘जुनुन’, ‘कलियुग’, ‘समर’ या फिर ‘सूरज का सातवां घोड़ा’। हर फिल्म एक अलग कैनवास और विषय पर खड़े होकर अलग तरीके से चिंता जताती है। पिछले कुछ सालों में आयीं उनकी फिल्में जैसे ‘जुबैदा’, ‘वेलडन अब्बा’ और ‘वेलकम टू सज्जनपुर’ इस बात को दिखाती हैं कि श्याम बेनेगल शिक्षित करने के साथ मनोरंजन का ताना-बाना भी बुन सकते हैं।
सुधीर मिश्रा
सुधीर मिश्रा का सिनेमा इंटलैक्चुअल और मेनस्ट्रीम सिनेमा का कॉकटेल है। ‘जाने भी दो यारों’ से सुधीर मिश्रा एक पटकथा लेखक के रूप में इंडस्ट्री में आए। यह 1983 का साल था जिस समय ‘हिम्मतवाला’ पैटर्न की फिल्में पसंद की जा रही थीं। ‘जाने भी दो यारों’ से सुधीर मिश्रा ने अपनी अलग तरह के सिनेमा की शुरुआत कर दी थी। ‘मोहनजोशी हाजिर हों’, ‘खामोश’, ‘इस रात की सुबह नहीं’ भी ऐसी ही कुछ अलग हटकर बनीं फिल्में थीं।
स्लम को फोकस करते हुए पर हॉलीवुड की फिल्म ‘स्लमडॉग मिलेनियर’ भले ही सुपरहिट रही हो पर शिल्प के मामले में सुधीर मिश्रा की फिल्म ‘धारावी’ उस पर 21 बैठती है। ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’, ‘खोया खोया चांद’, ‘ये साली जिंदगी’ और ‘इंकार’ जैसी फिल्में इस बात का इशारा करती हैं कर्मिश्यल तरीके से ट्रीटमेंट देकर भी एक अलग फिल्म फिल्म बनायी जा सकती है।
गोविंद निहलानी
गोविंद निहलानी का सिनेमा मनोरंजन करने के साथ-साथ कोई गंभीर बात चुपके से कहने का प्रयास करता है। सांप्रदायिकता और पुलिस के राजधर्म पर शायद सबसे अच्छी टिप्पणी गोविंद निहलानी की फिल्म ‘देव’ करती है। गोविंद निहलानी अपनी शुरुआत ‘आक्रोश’ फिल्म से करते हैं। उनकी फिल्म का नाम दरअसल उनकी मानसिक स्थिति को भी बयां करता है।
अस्सी के दशक में आयी यह फिल्म यथार्थ से दूर हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री को एक आईना दिखाती है। ‘आक्रोश’ के बाद ‘विजेता’, ‘अर्द्घसत्य’, ‘पार्टी’, ‘तमस’, ‘हजार चौरासी की मां’ और ‘तक्षक’ जैसी फिल्में एक अलग किस्म का सिनेमा रचती हैं। फिल्म मेकिंग स्टाईल में गोविंद निहलानी साहित्य और समाज दोनों से वास्ता दिखता है।
अनुराग कश्यप
21वीं शताब्दी में अलग तरह के सिनेमा बनाने में अनुराग कश्यप का नाम सबसे ऊपर आता है। लंबे समय तक दूसरे निर्देशकों के लिए फिल्म स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब अनुराग ने अपनी पहली फिल्म ‘पांच’ शुरू की तो यह फिल्म बनते-बनते बंद हो गयी। उनकी दूसरी फिल्म ‘ब्लैक फ्राइडे’ के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव हुआ। अनुराग ने हार नहीं मानी।
उन्होंने वैसा ही सिनेमा बनाया जैसा वह बनाना चाहते थे। ‘नो स्मोकिंग’ फिल्म बुरी तरह से पिटी लेकिन उसके बाद आयी फिल्म ‘देव डी’ सफल रही। अनुराग के लिए देव डी टर्निंग प्वाइंट थी। इसके बाद उन्होंने ऐसा सिनेमा बनाया जो उन्हें फिल्मीं भेड़चाल से अलग करता है। उनकी फिल्में ‘गुलाल’ और ‘उड़ान’ ने दिखाया कि सौ करोड़ के इस फिल्मी माहौल के बीच ही ऐसी फिल्में बनायी और चलायी जा सकती हैं। ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ बनाकर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्मी रेंज दिखायी है।
दिबाकर बनर्जी
फिल्मों की संख्या के मामले में दिबाकर बनर्जी छोटे हो सकते हैं लेकिन फिल्मों की समझ के मामले में नहीं। उनकी बनायी गयी फिल्मों की झलक देखिए। ‘खोसला का घोसला’, ‘ओए लकी लकी ओए’, ‘लव सेक्स और धोखा’ और फिर आखिरी में ‘शंघाई’। हर फिल्म का एक अलग समाज और कैनवास है। कॉमेडी करने का तरीका भी दूसरा और समाज की संड़ाध को दिखाने का भी।
‘शंघाई’ फिल्म बनाना एक साहस था, खासकार वैसे निर्देशक के लिए जिसकी अपनी जमीन भी उतनी पुख्ता नहीं हुयी थी। दिबाकर बनर्जी ने जब भी फिल्म बनायी उन्होंने एक छोटे से विषय या मानसिकता को बड़ा स्वरूप दिया। शायद यही उनकी यूएसपी है।